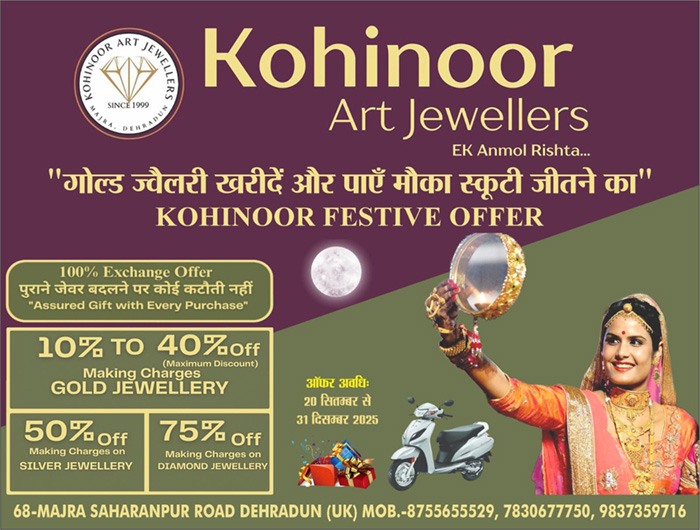resettlement (reverse migration)

देवेंद्र कुमार बुडाकोटी
पहाड़ों में एक राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र में एक छात्र ने मुझसे पूछा —“सर, क्या भविष्य में रिवर्स माइग्रेशन होगा?”
मैंने सीधा उत्तर दिया: नहीं।
उसके अगला सवाल पूछने से पहले ही मैंने कहा: “कोविड-19 के समय को याद कीजिए, जब कई लोग और परिवार अपने गांव लौट आए थे। लेकिन आज वे कहां हैं?”
ज्यादातर लोग फिर से अपने आजीविका स्थलों पर लौट गए हैं।
यह क्या दर्शाता है?
यह साफ तौर पर बताता है कि उस समय जो योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए थे, वे सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किए गए थे, उन्हें लागू करने में खामियां थीं और लोगों को वे आकर्षित नहीं कर पाए।
एक बार जब लोग शहरी जीवनशैली और सुविधाओं के आदि हो जाते हैं, तो उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ग्रामीण जीवनशैली में वापस ढलना मुश्किल हो जाता है — विशेषकर नई पीढ़ी के लिए।
शहरों में पल रहे बच्चों के लिए माता-पिता या दादा-दादी की गांव की कहानियां सिर्फ “कहानियां” रह जाती हैं — और वहीं कहानी खत्म हो जाती है।
जिन लोगों ने अपना बचपन या युवावस्था गांव में बिताई है, वही लोग गांव की यादों के प्रति सबसे ज़्यादा भावुक होते हैं।
तो, हमारा रिवर्स माइग्रेशन को लेकर क्या विज़न है? कि लोग गांव लौटें और खेती-बाड़ी या उससे जुड़ी गतिविधियों में लगें?
कोविड-19 के समय जो योजनाएं शुरू की गईं, वे मुख्यतः बागवानी, डेयरी, पशुपालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित थीं।
लेकिन सच यह है कि ज़मीन पर आधारित ये आजीविकाएं पहले ही अस्थिर हो चुकी थीं, क्योंकि ज़मीन अब बड़े परिवारों की खाद्य और चारे की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी।
ऐसे में जबरन कोई योजना गांव लौटे परिवारों पर थोपना उन्हें रास नहीं आया।
मसलन, बागवानी या मसाले जैसी नकदी फसलों के लिए बड़े स्तर पर खेती ज़रूरी होती है, लेकिन बिना चकबंदी (भूमि समेकन) के यह मुमकिन नहीं है।
बकरी पालन, डेयरी और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों के लिए बाज़ार से जुड़ाव और सप्लाई चेन बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादातर जगहों पर नहीं है।
इसके अलावा, इन प्राथमिक क्षेत्रों में योजनाएं फलदायी होने में समय लेती हैं। परिवारों के पास उतना धैर्य और संसाधन नहीं थे, इसलिए वे वापस अपने पुराने काम और स्थानों पर लौट गए।
हमें यह भी समझना चाहिए कि कोविड के समय जो लोग गांव लौटे थे, वे मुख्यतः असंगठित क्षेत्र से थे, जो शहरों में किराये पर रहते थे और जिनके छोटे बच्चे थे। इन बच्चों की पढ़ाई स्थान बदलने से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई।
लेकिन शहरी जीवनशैली की अभ्यस्त महिलाएं ग्रामीण सामाजिक परिवेश में सहज नहीं हो सकीं। बच्चे भी इस नये माहौल में ढल नहीं पाए।
एक समाजशास्त्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन में कोई रिवर्स गियर नहीं होता।
कुछ सफल रिवर्स माइग्रेशन के उदाहरण जरूर सामने आए हैं, लेकिन वे नियम नहीं, अपवाद हैं।
मैं उस भावना और नॉस्टेल्जिया को समझता हूं जो अतीत की स्मृतियों से जुड़ा है — और मैं स्वयं भी उन भावनाओं से जुड़ा हूं — लेकिन हमें सच का सामना करना चाहिए।
हम यह देख रहे हैं कि आज तो पास के छोटे शहरों से भी लोग गांव वापस नहीं लौटते — तो महानगरों या विदेशों से लौटने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
इस संदर्भ में नरेंद्र सिंह नेगी का गीत बेहद उपयुक्त लगता है:
“मुझे पहाड़ी-पहाड़ी मत बोलिए, मैं देहरादून वाला हूं।”
यह पंक्ति आज की स्थिति और मानसिकता को बखूबी दर्शाती है।
लेखक समाजशास्त्री हैं और विकास क्षेत्र में चार दशकों से अधिक समय से कार्यरत हैं।